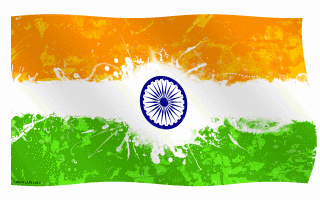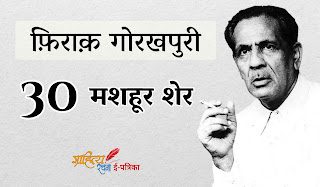दीपक राही - जम्मू कश्मीर
शिकार - कविता - दीपक राही
शुक्रवार, अक्टूबर 09, 2020
मुझे बहुत समझाया गया,
अगर अंधेरा हो तो,
घर से अकेले मत निकलना,
कभी कोई कुछ भी कहे,
तो चुप्पी साध कर आगे बढ़ना,
इन सब के बावजूद भी मै,
उनका शिकार हो ही जाती हूं,
बेटी, बेटा एक समान तो
कहा जाता है पर,
होते नहीं कभी,
मेरे जन्म होने से ही,
अपबाद खड़े हो जाते हैं,
बोझ सी लगती हूं,
इस समाज की रूढ़िवादी सोच को,
कितनी दरिंदगी है,
इस समाज में मेरे प्रति,
मेरी जीवा तक को काट दिया,
मेरे जिस्म और मेरे कपड़ों को,
इस तरह उधेड़ा गया कि जैसे,
कोई गिद्ध मृत पड़े हुए,
जानवर को बेरहमी से,
उधेड़ रही हो जैसे,
पर फिर भी इल्जाम,
मुझे पर जड़ दिए जाते हैं,
आखिर जिस्म तो था मेरा ही,
जो भेंट चढ़ा इन शिकारियों के,
मेरे जाने के बाद,
आंदोलन होंगे, मार्च निकलेंगे,
राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी,
कोर्ट कचहरी में केस चलेगा,
पर न्याय मिलते मिलते,
घरवालों के जूते घिस जाएंगे,
लोग अपने घरों को जाएंगे,
राजनेता वोट इकट्ठा करेंगे,
पत्रकार कुछ दिन खबर चलाएंगे,
साहब लोग आदेश का पालन करेंगे,
पर मैं एक बार फिर,
न्याय की चक्की में
सालों साल पिस्ती जाऊंगी।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर