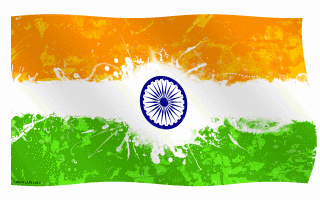एक बार फिर,
वही सवाल आया ?
कि आदमी जब,
जन्म लेता है,
और फ़िर मरता है,
तब वह नंगा,
क्यों दिखता है ?
कुछ भी तो उसके,
पास नहीं होता है।
सिर्फ और सिर्फ,
हाड़-मांस का लोथड़ा,
दिल की धड़कन,
और फिर उस कोमल,
आत्मा को ढंकती,
एक सुंदर- सी आकृति,
जिसका मां के गर्भ से,
बाहर आते ही,
उसकी पहचान,
सबसे पहले लिंग से,
होती है निर्धारित।
तत्पश्चात,
फिर प्रारम्भ होती है,
उसकी मौलिकता को,
अपने-अपने ही रंगों में,
रंगने का नायाब खेल।
पर उस में भी ,
मां बाप का
चलता है कहां जोर ?
क्योंकि पहले से ही,
उन पर जो ,
लगा रहता है ठप्पा,
उनके अबोध बच्चों पर भी,
वही सब हो जाती है चस्पा।
और फिर हो जाती है,
अबोध बच्चों की,
मन मस्तिष्क को,
कंडीशनिंग करने का,
गंदा और घिनौना खेल।
होंस संभालते ही,
उसके दिमाग में,
भर दी जाती है पहले,
अपने ही घरों में,
आइडेंटीफिकेशन की,
कुड़ा, करकट और भूसा।
और फिर,
उस भूसे को लेकर,
वह जिंदगी भर,
रहता है परेशान।
चाह कर भी,
वह उस भूसे से,
निकल नहीं,
सकता बाहर,
क्योंकि भूसों पर,
समाज की होती है,
कड़ी पहरेदारी।
पहरेदार की
आकाओं का भी,
रहता है अपना स्वार्थ,
उसे लगा रहता है,
हमेशा डर,
कहीं उसकी,
लूटिया ना,
हो जाए गुम।
इसलिए वह समाज में,
लोगों को लोगों से
अपनी ही फैलाई,
कुड़ा,करकट और ,
भूसों के बीच,
कुम्भला कर,
रखने के लिए,
भिन्न-भिन्न प्रकार की,
रंग-बिरंगी कसरतों का,
ज़ख़ीरा खड़ा कर,
उसकी आदमी पन की,
मौलिकता खत्म करने के लिए
सुबहो-शाम ,दिन-रात,
सचेत और संगठित हो,
पानी पी-पीकर,
करती रहती है,
अनथक प्रयास।
लेकिन जरा सोचिए,
और दिमाग पर,
बल लगाइए तो,
आदमी की आदमीयत,
खत्म करने की ,
उनकी सारी साजिशें,
धरी की धरी,
रह जाती है,
जब उसकी आत्मा,
अपनी पोशाक,
बदल रही होती है।
और जब श्मशान में,
वह जलकर,
भष्म बन जाती है,
तब कोई उसकी,
आइडेंटीफिकेशन,
चाहकर भी,
राख की ढेरों में,
ढूंढ़ नहीं पाती,
और ऐसे में फ़िर,
आदमी की आत्मा,
हो जाती पुनर्मूषको भव: ।
सुधीर कुमार रंजन - देवघर (झाड़खंड)