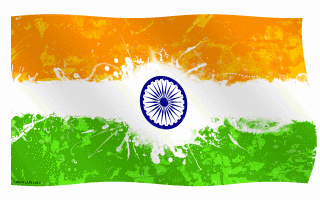डॉ. कुमार विनोद - बांसडीह, बलिया (उत्तर प्रदेश)
घर ! मुझे पहचानते हो - कविता - डॉ. कुमार विनोद
बुधवार, सितंबर 23, 2020
जीवन के आपाधापी में
शान्ति की तलाश में
इक्कीस दिनी शाश्वत् सत्य की खोज में
बाहर के अहर्निश शोर से अलग- थलग
एकान्त में रहने को मन आतुर
हो उठा
एक और शान्ति निकेतन की तलाश में
चम्पई रंग के उस अदभूत पलाश को देखने लगा
सोचा समुद्र की ओर
चला जाय तफरीह के लिए
लेकिन
घोर गर्जना करता
अट्टाहास करता
उसने कहा - मूर्ख !
भग जाओ यहाँ से
मैने जंगलों की ओर रुख किया
कभी सन्यासी धूनी रमाते थे यहाँ
पर यहाँ भी
इंसानी मस्ती में बस्ती हो गया
भागा पहाड़ की ओर
वहाँ भी .........
अन्ततः लौट आया
घर के सारे दरवाजे बंद क्रर दिये
बुझा दी सारी बत्तियां
नींद के बहाने
काल कोठरी सदृश
घर को ही क्वारेंटाइन बना डाला
जब सुबह उठा तो
झरोखे से आत्मीय किरणें मुझे
जगा रही थी
मुझे उत्तर मिल चुका था
अब और भटकना नही पड़ेगा
मिल गया चहारदीवारी वाला आत्मीय घर
सुस्वाद व्यंजन
माँ का ऑचल
जिसे सेनेटाइज करने की
कोई आवश्यकता नही
सुधि लेने वाले
टेलीफोनिक
ह्वाट्स अप्स,
मुख पोथी वाले सम्बन्धों की
आधुनिक उष्मा
मैने घर से पूद्दा
ओ मेरे अपने घर
मुझे पहचानते हो उसने तपाक से
गले लगा लिया ...... कहा-
सिर्फ इक्कीस दिन के लिये नही
ये तुम्हारा ही घर है
तुम्हारा अपना घर।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर