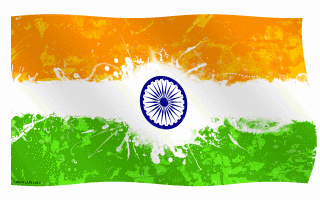सुषमा दीक्षित शुक्ला - राजाजीपुरम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
कम्बल - कविता - सुषमा दीक्षित शुक्ला
शुक्रवार, जनवरी 21, 2022
सर्द के दरमियाँ ये जो कम्बल है,
ये तो शीत इलाक़ों का सम्बल है।
उफ़ ये ठिठुरती फ़िज़ाएँ!
कंपकपाती सर्द घटाएँ!
कहीं बारिश, कोरोना, बर्फ़गोले,
लगता है फिर से रूठे हैं भोले।
निर्धन जन तो बस यूँ ही,
अनवरत टकटकी लगाकर,
ठिठुरती सदा को हलक में छुपाकर,
देखते भीगते आसमाँ को,
बस यूँ ही निरता-निरता कर,
ठिठुरन में धूप की उम्मीद जगाकर।
और फिर ओढ़ लेते ख़ामोशी की
मैली कुचैली फटी चादर को
अपना कम्बल मानकर।
जीर्ण शीर्ण काया को,
उसी अपने, कम्बल से लिपटाकर,
लरज़ते होठों और पथराते कपोलों को सिमटाकर,
मन ही मन कहते एक अनकही
अनसुनी गुहार लगाकर,
हे सूर्य देव! हे अग्नि देव!
प्रभु दया दृग खोलो।
कम्बल में अब ऊष्मा नहीं,
पतीले में अब दाना नही।
भेज दो किसी अमीर को,
भूख और शीतलता हरने,
कम्बल, कैमरा व चावल के साथ।
उसे शोहरत नसीब हो,
और मुझे थोड़ा जीवन।
या प्रभु! स्वयं बिखर जाओ,
ढक लो धरा को ऊष्मा बनकर,
एक प्राकृतिक अमूल्य कम्बल से,
हर लो यातनाएँ अटूट सम्बल से।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर