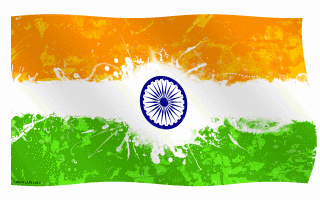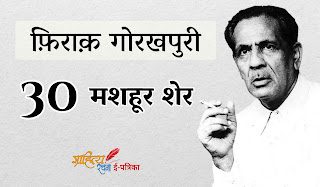विकाश बैनीवाल - भादरा, हनुमानगढ़ (राजस्थान)
ज़िंदगी बसर कर - कविता - विकाश बैनीवाल
सोमवार, जून 07, 2021
इतना नाज़ुक नहीं तन
मामूली आग से राख हो जाए,
यह राख तज़र्बों की ढेरी है।
इधर रेत फिसली मुट्ठी से
गर्म-गर्म हवा निकली,
बे-वक़्त कंबल ओढ़ सो गया।
ताज्जुब हुआ कायनात को
शरीर ख़ाक ना हुआ,
वक़्त रहते उठ गया।
ख़फ़ा हुआ जो मयख़ाने से
मौत का नशा चढ़ गया,
हर दफ़ा यूँ बच कर निकला।
मौत की गिरफ़्त ढीली पड़ी
गीली लकड़ियों की सख़्ताई,
उससे दफ़नाया भी न गया।
नज़रें इनायत ख़ुदा की
पड़ी जो जो कोने किनारे,
रहम बख़्शी मालिक ने।
तलब लगी थी मौत देखने की
सबब ना मिला तलब का,
फ़रमाया आख़िरी ख़्वाहिश थी!
चिलमन से झाँका एक बार
फिर आमीन कह टाल दिया,
जो ताबीर निकले ज़िंदगी का।
आख़िरी फ़ैसला होगा कभी तो
मसरूर रहे पल पल,
'विकासा' फिर ज़िंदगी बसर कर।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर