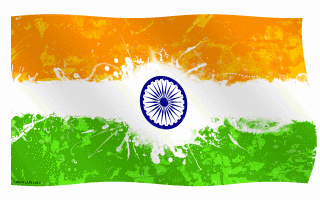गोपाल मोहन मिश्र - लहेरिया सराय, दरभंगा (बिहार)
ज़िम्मेदारी - लघुकथा - गोपाल मोहन मिश्र
शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021
समय भले ही बीत जाए, हमारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं बदलतीं। बस उन्हें समझना होता है। हर सुबह हंगामा होता था। तीन वर्ष की शुचि को स्कूल भेजना एक युद्ध के समान था।
उसके माता-पिता नौकरी पर निकल जाते थे। घर में रह जाते थे दादा और दादी। दादा डॉक्टर थे। सो सुबह से ही मरीज़ों में व्यस्त हो जाते थे। बेचारी दादी किसी तरह शुचि को तैयार करके स्कूल भेजतीं।
समय बीतता गया। शुचि बड़ी होने लगी। दादी बूढ़ी होने लगी। धीरे-धीरे शुचि ठीक-ठाक स्कूल जाने लगी। फिर कॉलेज जाने लगी। फिर नौकरी करने लगी। फिर शादी हो गई। शादी उसी शहर में हुई थी।
अब समय ठीक उल्टा हो गया था। दादी बहुत बूढ़ी हो गई थीं। उन्हें सम्भालना एक कठिन काम होता जा रहा था। शुचि रोज़ सुबह आती, उन्हें तैयार कर काम पर निकल जाती। फिर अपने घर जाकर वहाँ सब सम्हालती। फिर वापस आकर दादी को सम्हालकर अपने घर चली जाती।
शुचि के पति ने एक दिन पूछा- "तुम रोज़ अपने मायके क्यों जाती हो? वहाँ एक नौकरानी रख दो। वह सब सम्हाल लेगी।" शुचि ने सिर तानकर कहा- "जिस दादी ने मेरा बचपन सम्हाला था, उनका बुढ़ापा सम्हालना आज मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी है।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर