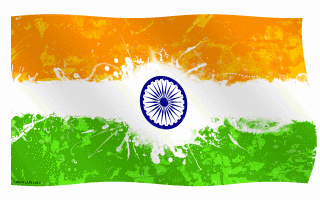कर्मवीर सिरोवा - झुंझुनू (राजस्थान)
संघर्ष - कविता - कर्मवीर सिरोवा
गुरुवार, अक्टूबर 15, 2020
पिता के खुरदरे पैर
जैसे ही दहलीज पर घर्षण करते थे,
घर में वो निढ़ाल जिस्म
एक ऊर्जा ले आता था।
तिरपाल जैसी चुभती शर्ट
ऐसे भीगी होती थी जैसे
झाड़ पर ठहरी हो कोई शबनम।
पसीनें की लहलहाती महक,
चूल्हें की बुझती लौ में घी झोंक देती थी।
पसीनें की बूँदों से,
मेरे छोटे से जिस्म की जड़े पल रही थी।
चारपाई की टूटती जड़ें
जमीन को छूकर जताती कि
इस संघर्ष ने थका दिया हैं पिता को,
पर रुकना कहाँ था संघर्ष अविराम था।
ये संघर्ष था कि चूल्हा सुलगता रहें,
मेरी भारी भरकम किताबें आती रहें।
फूल स्पीड में चलते पंखे ने
जैसे जानबूझकर
अखबार का पेज पलटा,
तो अखबार पिता का संघर्ष दिखा रहा था,
छपा था कि गर्मी ने इस बार भी
सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये।
वो संघर्ष ही था कि पिता ने
महीनें के पूरे तीसों दिन,
तपती धूप को दे दिए,
पिता ने सूरज का घमंड तोड़कर,
खुद को जला दिया,
पर मुझें ऑफिस में बैठा दिया।
ये संघर्ष इतना नम था,
कि आज जब सोचता हूँ
इस संघर्ष के बारे में,
आँखों से टपक जाता है पसीना।।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर