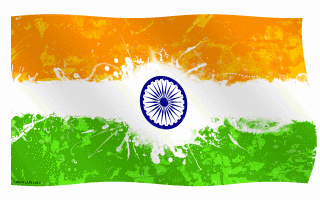मंजरी "निधि" - बड़ोदा (गुजरात)
मेला - लेख - मंजरी "निधि"
मंगलवार, अप्रैल 06, 2021
मेला यह शब्द सुनते ही ढेरों यादें और एक विस्तृत चित्रण आँखों के सामने ऐसा आता है कि वो प्रत्यक्ष लगने लगता है। मेले के नाम से एक रोमांच आ जाता है। मेला शब्द सुनते ही वो रंग बिरंगी पोशाकें, वो खनखनाती चूड़ियाँ, वो डिब्बे वाला सिनेमा, वो झूलो से डर की वजह से चिल्लाने की आवाज़ें, वो मिठाई की दुकाने, वो लकड़ी की पालकी वाले झूले की चरचराहट की आवाज़, वो चाट के ठेले, वो मौत का कुआँ, वो रावण का अटट्टाहास, वो लाउड स्पीकर पर एक के सात एक के सात की आवाज़ें, वो धक्का मुक्की ये सब कोई कैसे भूल सकता है?
मेला एक ऐसा आयोजन है जिसमें मिलन सगे सम्बन्धियों का, मिलन व्यापारी वर्ग का, मिलन जवान हृदयों का, मिलन कलाबाज़ी दिखाने वालों का, मिलन दूर दराज़ों के परिचितों का, मिलन रिश्तेदारों का, मिलन दोस्त यारों का।
मेले की तैयारी में मैदान साफ किए जाते थे, सामान से लदे बहुतायत में वाहन आते थे, तम्बू लगते थे, बड़े बड़े बैनर्स सजते थे। ये सारा साल में एक बार ही देखने को मिलता था। हम कौतूहलवश एक दो दिन छोड़ शाम को मेले के स्थान पर मुआयना कर आते थे।
मेला हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है पर हाल फ़िलहाल हम उसे था ही मानेंगे क्यूँकि अब मेले लुप्त से होते जा रहे हैं। हमारे देश में मेले को एक उत्सव जैसा मानते थे। मेला एक जीवन संस्कृति थी। यह एक ऐसा अवसर होता था जहाँ मनुष्य कम पैसे में या बिना पैसों के भी मेले की रौनक़ देखकर दिल बहला सकता था। सारे उम्र के लोग मेले में जाकर उसका आनंद उठा सकते थे। उन दिनों देश में बहुत सारे मेले लगते थे। सारे मेलों की अपनी एक अलग संस्कृति थी। हरेक जात, हरेक कोम, हरेक प्रदेश अपनी ज़रूरत अनुसार मेले का आयोजन करता था। कहीं सिर्फ जानवरों का मेला लगता जैसे- बैल, गाय घोड़े, ऊँट आदि। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि गधों के भी मेले लगते थे। इन गधों को भी अच्छे से सजाया सँवारा जाता था। मेला सारी महिलाओं का एकमात्र मिलन स्थल हुआ करता था। महिलाओं को मेले के नाम पर घर से निकलने की आज़ादी हुआ करती थी। देश के दुर्गम गाँवों में बसे सभी उम्र के लोग इन मेलों का बेसब्री से इंतज़ार करते क्यूँकि उनके पास मनोरंजन का कोई दूसरा साधन जैसे सिनेमा या नाटक उपलब्ध नहीं होते थे। मेला शुरू होने के आठ दस दिन पहले से ही बच्चों का उत्साह चरम सीमा पर होता था। मेले के लिए नये कपड़े खरीदना, खरीदने की वस्तुओं की सूची तैयार करना, गुल्ल्क में पैसे जोड़ना आदि। मेले अधिकतर त्योहारों या फिर मौसम के हिसाब से लगते थे। दीपावली के बाद लगने वाले मेले में गेहूँ, सूखे मसाले-हल्दी, लाल मिर्च, खड़ा धना बिकते थे। लोग साल भर के मसाले, अनाज खरीद लेते थे। एक तरफ़ लोग खरीद में व्यस्त रहते थे तो दूसरी तरफ़ मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे। वहाँ लोग कौतूहलवश बैठते थे। मौत के कुए में घूमती मोटर साइकिल, लोकगीतों पर नृत्य, झूलों पर झूलने लगी कतारें, ढोलक पर दंगल का शोर, संध्या बेला में भजनों की आवाज़ें और सीता हरण पर दर्शकों का विलाप। कुछ मेलों में स्वयंवर भी होते थे जहाँ वधुएँ अपने वर पसंद करतीं थीं। जैसे जैसे समय बदलता गया मेलों का रूप भी बदलता गया। बड़े शहरों से तो मेले विलुप्त ही हो गए।
आज हर कॉलोनी के बगीचों में, एम्यूजमेंट पार्क्स में झूले लग गए। मेले की जगह मॉल ने ले ली। पर मॉल में ना तो वो आत्मीयता है ना ही वो अपनापन। वहाँ है तो सिर्फ़ पश्चिमीकरण, सिर्फ छलावा। आज ऑनलाइन खरीदी का दौर शुरू हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना ऑनलाइन उद्योग बढ़ा रहीं हैं। ऐसे में राशन की दुकान वाले लाले और मॉल से भी खरीदी कम हो गई हैं। जनता अपने गाँवों की तरफ़ लौट रही है। अभी भी मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम वापस फिर वही लम्हे, वही मेले जी पाएँगे...?
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर