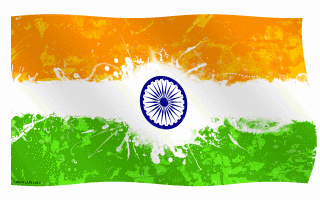विभान्शु राय - ग़ाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश)
धर्म बनाम कर्म : विचार और क्रियान्वयन
गुरुवार, नवंबर 20, 2025
विचारों का उद्गम हमेशा किसी बड़े अवसर से नहीं होता, कई बार किसी क्षणिक प्रश्न से ही विचारों की एक नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है-अनायास, पर अनंत। ऐसा ही एक प्रश्न कभी मेरे जीवन के एक सहज क्षण में उठा था, जिसने धर्म और कर्म के प्रति मेरे दृष्टिकोण की नींव रखी और जो आज के हमारे इस चिंतन का मूल आधार बना है।
मुझे आज भी स्मरण है - लगभग तीन वर्ष पूर्व का वह क्षण, जब मैं बारहवीं कक्षा का विद्यार्थी था। हिन्दी की कक्षा चल रही थी - विषय था गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। मैं और मेरा एक मित्र दाईं पंक्ति की पीछे की मेज़ पर बैठे थे, और चर्चा एक सवैया पे चल रही थी जिसमें गोस्वामी जी तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों, जैसे जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता और नैतिक पतन पर कड़ा प्रहार करते हैं। चर्चा के उसी क्रम में मेरे मित्र की किसी टिप्पणी पर अध्यापिका ने उससे प्रश्न किया - "तुम्हारे विचार में आज के वैज्ञानिक युग में, जब तकनीक और तर्क हर क्षेत्र में मार्गदर्शक है, धर्म का अधिक महत्व है या कर्म का?"
मित्र ने अपने विवेकानुसार उत्तर दिया, जो विचार की दृष्टि से तो सार्थक था, परन्तु उसके उत्तर में वह दृढ़ता और गहराई नहीं थी, जिसकी इस प्रश्न को आवश्यकता थी। शायद उस उत्तर से उपजे हल्के से असंतोष ने मेरी चेतना की भूमि पर धर्म और कर्म के उस प्राचीन परंपरागत वैचारिक द्वंद्व का बीज एक स्वाभाविक जिज्ञासा के रूप में अंकुरित कर दिया। इस जिज्ञासा ने मुझे धर्म और कर्म के अंतर्निहित संबंध को समझने के लिए हमेशा प्रेरित किया।
हमारे भारतवर्ष में, जो एक कर्मप्रधान और धर्मप्राण राष्ट्र है, यहाँ धर्म और कर्म का एक प्राचीन, नैसर्गिक संबंध हमेशा से ही विद्यमान रहा है। परन्तु उसके साथ ही सामान्य मानव मन में इनके बीच समन्वय, श्रेष्ठता और प्रासंगिकता को लेकर एक किस्म का गहन द्वंद्व भी हमेशा उपस्थित रहा है। कभी धर्म को सर्वोच्च मानकर कर्म की भूमिका को सीमित किया गया, तो कभी केवल कर्म को प्राथमिकता देते हुए धर्म के नैतिक पहलुओं पर प्रश्न उठाए गए।
जीवन के हर आयाम में, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत हो, धर्म और कर्म का परस्पर संबंध हमारे आचार, निर्णय और व्यवहार का आधार रहा है। यह द्वंद्व आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन और समाज के नैतिक निर्णयों में सक्रिय रूप से महसूस किया जा सकता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न होता है - यदि धर्म और कर्म दोनों हमारे जीवन के मूल आधार हैं, तो उनके बीच यह निरंतर संघर्ष और संतुलन की चुनौती क्यों बनी रहती है, और अंततः दोनों में से कौन श्रेष्ठ है?
वास्तव में, जो लोग केवल धर्म अथवा केवल कर्म को ही मानने की बात करते हैं, वे प्रायः धर्म के वास्तविक अर्थ और उसके कर्म से जुड़े मूल भाव को लेकर एक गलत अवधारणा रखते हैं। आज के इस चिंतन के माध्यम से हम धर्म और कर्म के वास्तविक अर्थ, उनके उद्देश्य और उनके पारस्परिक संबंध की उस गहराई को समझने का प्रयास करेंगे, जो मानव जीवन की पूर्णता और सार्थकता का मूल है।
'धर्म' शब्द सुनते ही, हममें से अधिकांश लोग उसे 'रिलिजन' (Religion) का पर्याय मान लेते हैं, और इस एक भ्रांति में उस शब्द के व्यापक, गहन और सार्वभौमिक अर्थ को अत्यंत संकीर्ण दायरे में बाँध देते हैं। 'Religion' शब्द का अर्थ किसी विशेष पंथ, संप्रदाय, विश्वास या मज़हब तक सीमित रह जाता है। लेकिन 'धर्म' इससे कहीं अधिक व्यापक है - यह केवल विश्वास या परम्परा नहीं, बल्कि जीवन की नींव तथा आचरण की दिशा से जुड़ा एक सारगर्भित मूल्य है। 'धर्म' शब्द के साथ जो त्वरित संकल्पना हमारे मानस-पटल पर उद्भासित होती है, वह प्रायः पूजा-पाठ और कर्म-कांड के उस संस्थागत रूप में होती है, जबकि धर्म का वास्तविक आयाम इससे कहीं अधिक गहन है।
वास्तव में 'धर्म' शब्द संस्कृत भाषा की 'धृ' धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है धारण करना या धारण करने योग्य ।
महाभारत में धर्म के इसी मूल तत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है
"धारणाद्धर्म इत्याहु र्धर्मो धारयते प्रजाः।
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः॥"
अर्थात्, धर्म वह है जो धारण करता है - जो जीवन, समाज और सृष्टि को स्थायित्व, संरक्षण और संतुलन प्रदान करता है। वह शक्ति, जो समस्त प्राणियों और सृष्टि को एक सूत्र में बाँधकर स्थित रखती है या धारण करती है, वह निश्चित रूप से धर्म है।
'धारण' की इस व्याख्या से एक स्वाभाविक प्रश्न उभरता है आख़िर क्या धारण करना धर्म है? वह कौन-सी सत्ता, कौन-सा तत्व या आचरण है जिसे धारण करना ही धर्म कहलाता है?
यह प्रश्न हमारी आंतरिक चेतना को स्पर्श करता है और हमें यह समझने की ओर उन्मुख करता है कि धर्म वस्तुतः उन जीवन मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों तथा व्यक्तिगत व्यवहार या आचरण के उन समस्त नियमों का धारण है, जिनके पालन से मनुष्य की चेतना नैतिकता और आध्यात्मिकता के आधार पर संयमित होती है। इन नियमों से समाज में वह आंतरिक एकसूत्रता, संतुलन और सद्भाव बना रहता है, जो उसे विखंडन से बचाकर एक जीवंत, संगठित और समरस स्वरूप प्रदान करता है। धर्म, बाह्य विचार या अनुष्ठान की औपचारिकता नहीं, बल्कि वह अंतःशक्ति है जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायी बनाती है।
उदाहरणार्थ, मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षणों का उल्लेख मिलता है, जो यह स्पष्ट करते हैं की धर्म का वास्तविक स्वरूप किन गुणों या आचरणों में निहित है -
"धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणं॥"
अर्थात् - धृति (धैर्य), क्षमा-शीलता, दम (आत्मसंयम), अस्तेय (चोरी ना करना), शौच (आंतरिक एवं बाह्य शुद्धता), इंद्रियनिग्रह (इंद्रियों पर नियंत्रण), धी (सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना), विद्या (यथार्थ ज्ञान), सत्य (सत्यवादिता) और अक्रोध (क्रोध का अभाव ) - ये धर्म के दस लक्षण माने गए हैं।
ये लक्षण व्यक्ति को परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव में स्थिर रखते हैं, उसके आचरण में पवित्रता और निष्कपटता का संचार करते हैं तथा उसकी बुद्धि और वाणी को मर्यादित करते हुए उसे सत्य के मार्ग पे स्थिर रखते हैं। इस प्रकार, धर्म किसी उपासना-पद्धति का बंधन नहीं, बल्कि चरित्र, संयम और करुणा का वह समन्वित भाव है जो व्यक्ति को भीतर से प्रकाशित करता है और समाज को बाहर से सुव्यस्थित रखता है। धर्म की यही आंतरिकता उसे कालातीत बनाती है – क्योंकि जहाँ तक मनुष्य रहेगा, वहाँ तक इन मूल्यों की आवश्यकता भी बनी रहेगी।
धर्म का यह आंतरिक स्वरूप स्पष्ट करता है कि वह केवल विचार या बोध का विषय नहीं, बल्कि जीवन में क्रियान्वित होने वाली चेतना है। तभी यह प्रश्न उभरता है धर्म का असली मूल्य कर्म में, उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में कैसे प्रकट होता है? यही वह बिंदु है जहाँ धर्म और कर्म के बीच के बीच का सूक्ष्म अंतर और उनके बीच का गहन संबंध उद्घाटित होता है और यही चर्चा हमें अगला आयाम देती है। कर्म' शब्द संस्कृत की “कृ” धातु से उत्पन्न है, जिसका अभिप्राय है - कार्य या क्रियाशील होना। यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहन है।
सामान्यतः हम कर्म को केवल किसी कार्य, क्रिया या व्यवहार के रूप में देखते हैं, परंतु उसके अर्थ की गहराई इससे कहीं अधिक है। भारतीय दर्शन में कर्म का अर्थ केवल क्रिया मात्र नहीं है। यह न केवल "क्या किया गया", बल्कि "क्यों किया गया" और "किस भावना से किया गया” – इन तीनों का सम्मिलित मूल्यांकन है।
कर्म की यही व्यापकता उसे केवल बाह्य क्रियाओं से ऊपर उठाकर, एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत का रूप देती है। कोई भी कार्य तभी "कर्म” कहलाता है जब उसमें सचेत इच्छा, उद्देश्य और मूल्य निहित हों। कर्म वही है जो चेतन भागीदारी और नैतिक उत्तरदायित्व से सम्पन्न हो।
मनुष्य का हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया - कर्म का ही एक सूक्ष्म रूप है। भगवद्गीता के अनुसार, कर्म मनुष्य के अस्तित्व का स्वाभाविक और अविभाज्य अंग है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है
"न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥"
(अध्याय 3, श्लोक 5)
अर्थात् – कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। उसके भीतर का समस्त चेतन तंत्र - शरीर, मन और बुद्धि - प्रकृति के तीन गुणों (सत्व, रज और तम) से संचालित होकर अनिवार्य रूप से संसार में कर्म करने के लिए प्रेरित और बाध्य होता है।
जैसा कि हमने देखा, भारतीय दर्शन केवल कर्म की बाह्य क्रियाओं पर ही नहीं, बल्कि कर्म में निहित भावना, उद्देश्य और बोध पर भी विशेष जोर देता है।
इसी दृष्टि से भगवद्गीता कर्म की अनिवार्यता के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करती है कि कर्म तभी सार्थक है जब वह सही भावना और सचेत बोध से संपन्न हो। गीता में इस गहन सत्य को निष्पादित करते हुए कहा गया है
"कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥"
(अध्याय 4, श्लोक 17)
अर्थात् – केवल "कर्म करना या न करना" ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मनुष्य को कर्म (धर्मानुसार सही कार्य), विकर्म (धर्मानुसार गलत कार्य) और अकर्म (कर्म का त्याग या निष्क्रियता) - तीनों को भलीभाँति समझना चाहिए। अतः कर्म का आशय केवल किसी कार्य के निष्पादन से नहीं, बल्कि उस चेतन प्रवृत्ति से है, जो किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जागृत होती है। जब यह प्रवृत्ति लोकहित, न्याय और सत्य के संयोग से संबद्ध होती है, तब वही 'धर्म' का रूप धारण कर लेती है।
यही वह बिंदु है जहाँ धर्म और कर्म का संगम होता है। वास्तव में, धर्म का असली मूल्य तभी प्रकट होता है जब वह कर्म के माध्यम से व्यवहार में उतरता है। केवल ग्रंथों में अंकित या वचनों में उच्चारित धर्म, यदि कर्म में परिणत न हो, तो वह निर्जीव अवधारणा मात्र रह जाता है। कर्म ही धर्म को जीवन देता है - वह धर्म को सैद्धांतिक से व्यावहारिक, अमूर्त से मूर्त बनाता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में न्याय, सत्य, करुणा और समर्पण को अभिव्यक्त करता है, तभी उसका धर्म सजीव होता है।
चाहे वे श्रीराम हों, श्रीकृष्ण हों, गौतम बुद्ध हों, या वे अन्य तमाम महापुरुष, जिन्हें आज हम एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं- इन सभी ने एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया, अपने कर्म के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण किया, और अपने उस दृढ़ चरित्र तथा अडिग आचरण के माध्यम से एक कालजयी विचार बनकर हमारे बीच प्रतिष्ठित हैं।
और जो लोग धर्म और कर्म के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न उठाते हैं, मेरे विचार में यह प्रश्न ही निरर्थक है – क्योंकि श्रेष्ठता वहाँ तय होती है जहाँ भिन्नता हो, जबकि धर्म और कर्म के अस्तित्व में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि परस्पर पूरकता है।
धर्म का सार कर्म में निहित है, और कर्म का पवित्रतम स्वरूप वही है जिसमें धर्म की आत्मा निवास करती है। दोनों का यह समन्वय ही मानव जीवन को अर्थ, दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है।
मैं किसी अन्य संप्रदाय या उनके विश्वासों की बात नहीं करूँगा, परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म और भारतीय हिन्दू दर्शन में कर्म को हमेशा विशेष महत्व दिया गया है।
हिन्दू दर्शन ने सदैव विचार और बोध की स्वतंत्रता को महत्व दिया है। कुछ ग्रंथों में वर्णित विश्वासों को कठोरता से मानने के बजाय, यह दर्शन तर्क, विवेचना और अनुभव में विश्वास करना प्रोत्साहित करता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है।
अंततः मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म केवल कोई पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन-पद्धति है।
साहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos
साहित्य रचना कोष में पढ़िएँ
विशेष रचनाएँ
सुप्रसिद्ध कवियों की देशभक्ति कविताएँ
अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति कविताएँ
फ़िराक़ गोरखपुरी के 30 मशहूर शेर
दुष्यंत कुमार की 10 चुनिंदा ग़ज़लें
कैफ़ी आज़मी के 10 बेहतरीन शेर
कबीर दास के 15 लोकप्रिय दोहे
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? - भारतेंदु हरिश्चंद्र
पंच परमेश्वर - कहानी - प्रेमचंद
मिर्ज़ा ग़ालिब के 30 मशहूर शेर